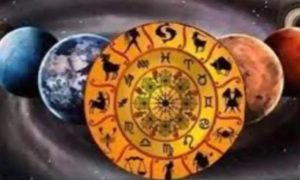अरविंद मिश्र। स्काटलैंड का ग्लासगो शहर दुनिया भर के पर्यावरण और ऊर्जा प्रतिनिधियों की मेजबानी को तैयार है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में बंदरगाहों के इस शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन ‘काप-26’ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें मानवीय जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ऊर्जा संसाधन एवं परियोजनाएं चर्चा के केंद्र में रहेंगी। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को दिशा देने वाले इस महाआयोजन से ठीक पहले भारत और चीन समेत यूरोपीय देशों से ऊर्जा संसाधनों में असंतुलन की आहट सुनाई दे रही है। भारत में यह कोयला संकट के रूप में है तो यूरोपीय देश प्राकृतिक गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में ऊर्जा संसाधनों के संकट की हालिया वजह भले ही परिस्थितिजन्य हो, पर कुछ ही ऊर्जा स्नेतों पर बढ़ती निर्भरता भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी है।
खनन पर आर्थिक अनिश्चितता का असर : देश में कोयले के कथित संकट को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। कुल बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा कोयला आधारित परियोजनाओं पर निर्भर है। यही वजह है कि कोयला संकट का करंट हर जगह महसूस किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल तो इसमें पालिटिकल माइलेज भी तलाश रहे हैं। कोयले की आपूर्ति और मांग में अचानक आए अंतर की सबसे अहम वजह कोरोना काल की आर्थिक अनिश्चितता से खनन में आई गिरावट, राज्यों की ओर से लंबित भुगतान और आयातित कोयले की दरों में वृद्धि है। पूर्णबंदी की आर्थिक सुस्ती के बाद अब बिजली की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं आर्थिक अस्थिरता की आशंका से कोयले की मांग और उसके भंडारण का सही आकलन नहीं हो पाया। कई कोयला उत्पादन कंपनियों ने पिछले साल जो आपूर्ति की थी, उसका बिजली संयंत्रों द्वारा समय पर भुगतान न होने से समस्या और बढ़ गई। ऐसे में विगत एक साल से आर्थिक नुकसान ङोल रहीं कोयला कंपनियां लंबित देनदारी खत्म करने के बाद ही खनन शुरू करने की रणनीति पर काम करने लगीं। इस वर्ष कोरोना काल में श्रमिकों के पलायन और मानसून के दौरान कोयला खदानों में जल भराव ने भी कोयले के आपूर्ति तंत्र को बाधित किया है। इसके कारण जहां खनन कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा, वहीं पर्याप्त श्रमिक न होने से भी खनन कार्य प्रभावित रहा।

अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ी मांग : कोरोना काल के बाद भारतीय अर्थतंत्र में बिजली समेत सभी आठ बुनियादी क्षेत्रों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में देश की जीडीपी पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज कर चुकी है। इस दौरान खनन क्षेत्र में 18.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में बिजली की खपत अगस्त-सितंबर 2021 में 124.2 अरब यूनिट हुई है, वहीं अगस्त 2019 में यह 106.6 अरब यूनिट थी। कोयले की आपूर्ति में आई तात्कालिक रुकावट को समझने के लिए जरा कोविड काल की परिस्थितियों को याद करें। पहले और दूसरे चरण के लाकडाउन के दौरान देश में बिजली की खपत पिछले कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। जाहिर है जब बिजली की खपत कम होगी तो उसका उत्पादन और उसके लिए जरूरी कच्चे माल की मांग में कमी आएगी। इस बीच विदेश से आयात होने वाले कोयले की कीमत में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका, आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से कोयला आयात करता रहा है। मार्च 2021 में इंडोनेशियाई कोल की कीमत 4,500 रुपये प्रति टन थी, जो सितंबर-अक्टूबर में बढ़कर 15,000 रुपये प्रति टन हो गई। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने कोयले का घरेलू मोर्चे पर ही उत्पादन बढ़ाने की रणनीति को प्रोत्साहित किया। इससे 2019 की तुलना में आयातित कोयले से बिजली के उत्पादन में 43.6 प्रतिशत की कमी आई है।

समन्वय से ही निकलेगा समाधान : देश में 135 तापीय बिजली संयंत्र हैं। सामान्य स्थिति में सभी संयंत्रों को पंद्रह से बीस दिन का कोयला भंडार रखना होता है, लेकिन 72 तापीय बिजली संयंत्रों के पास तीन दिन का कोयला स्टाक है। 50 संयंत्रों के पास चार से दस दिन और दस संयंत्रों के पास दस दिन से अधिक का कोयला उपलब्ध है। वर्तमान में देश में कोयले की रोजाना खपत 16.8 लाख टन है, जबकि रोजाना आपूर्ति 15.7 लाख टन है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला उत्पादक देश भारत में इस वर्ष कोयले का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। कोयला मंत्रलय के मुताबिक कोल इंडिया के पास 4.3 करोड़ टन कोयला उपलब्ध है, जो बिजली संयंत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। कोल इंडिया वर्तमान भंडार से 24 दिनों के कोयले की मांग पूरी कर सकती है। खास बात यह है कि देश में बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले की खान के पास हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थित थर्मल पावर प्लांट इसके उदाहरण हैं। इन विद्युत संयंत्रों को कोयले का अतिरिक्त स्टाक रखना जरूरी नहीं होता है। कोयला खानों के पास स्थित बिजली संयंत्रों में रोजाना की जरूरत के मुताबिक ही कोयले की आपूर्ति होती है। इसके साथ ही देश में कई तापीय विद्युत संयंत्रों के पास अपनी कोयला खान हैं। ऐसे में कोयले के स्टाक को लेकर कुछ राज्य सरकारों और दलों की ओर से राजनीतिक करंट पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, वह तथ्यों में निराधार ही नजर आती है।
कोयले के इस अल्पकालिक संकट पर केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। इस दिशा में मोदी सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उनमें कोयले का खनन बढ़ाने के साथ ही रेलवे से बिना रुकावट के तीव्र परिवहन की अनुमति प्रमुख है। केंद्र के स्तर पर एक अंतरमंत्रलयी उप समूह सक्रिय है। यह समूह दैनिक आधार पर कोयला स्टाक की निगरानी और प्रबंधन कर रहा है। कोयला मंत्रलय, रेलवे और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का असर भी दिख रहा है। नई खदानों को पर्यावरणीय एवं अन्य मंजूरी दिलाकर तीव्र उत्खनन की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत : भारत में कोयला संकट अल्पकालिक इसलिए बताया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने रणनीतिक रूप से आयातित कोयले पर तो निर्भरता कम की है, वहीं समानांतर रूप से नई खनन परियोजनाओं को उत्खनन की मंजूरी भी प्रदान की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में ही कोल इंडिया ने 32 खनन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनसे 2023-24 तक लगभग 8.1 करोड़ टन कोयले का सालाना अतिरिक्त उत्पादन होगा। सरकार के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान बिजली क्षेत्र को 70 करोड़ टन से अधिक कोयले की आवश्यकता होगी। वर्ष 2020 कोयला क्षेत्र में हुए नीतिगत सुधारों के लिए जाना जाएगा। पिछले वर्ष ही निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक कोयला उत्खनन में प्रवेश देने के लिए कोयला ब्लाकों की नीलामी हुई है। बिजली उत्पादन में कोयले पर हमारी निर्भरता भले ही दो-तिहाई से अधिक हो, लेकिन देश में बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी भी पिछले कुछ वर्षो में बढ़ी है।
वर्तमान में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा स्नेतों की लगभग 90 हजार मेगावाट से अधिक हिस्सेदारी है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले पांच वर्षो में हमारी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 162 प्रतिशत बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट और 2035 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। प्राकृतिक गैस से बिजली तैयार करने वाले संयंत्रों में निवेश बढ़ रहा है। अकेले एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली स्टेशन 4,017.23 मेगावाट बिजली तैयार कर रहे हैं। इसी तरह गैस आधारित संयुक्त उद्यम 2,494 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। वन नेशन वन गैस ग्रिड के जरिये गैस आधारित बिजली परियोजनाओं के लिए अबाध प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। ये तमाम उपाय भारत ही नहीं, किसी भी विकासशील देश की ऊर्जा टोकरी को टिकाऊ बनाएंगे। हालांकि हरित ऊर्जा अथवा ऊर्जा संसाधनों की विविधता का कोई भी प्रयास बड़े निवेश और आधुनिक तकनीक के समावेश से ही संभव होगा।
स्पष्ट है ऊर्जा के मौजूदा संकट के दीर्घकालिक समाधान के लिए ऊर्जा विविधीकरण की राह पर आगे बढ़ना होगा। हरित ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाना समय की मांग है, पर प्राकृतिक गैस और अक्षय ऊर्जा की अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में ऊर्जा के हर कच्चे माल का न्यायसंगत समायोजन करना होगा। यह तभी संभव है जब आर्थिक महाशक्तियों के साथ विकासशील और पिछड़े देशों के बीच ऊर्जा की ठोस साङोदारियां विकसित हों।
जलवायु परिवर्तन के लिए ठोस उपाय खोजने के चलते आज दुनिया ऊर्जा के ऐसे संक्रमण काल में पहुंच गई है, जहां हर देश नई ऊर्जा चुनौतियों से जूझ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह कई आर्थिक महाशक्तियों की जलवायु परिवर्तन के मामले में एकला चलो नीति भी है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां जलवायु परिवर्तन पर मची होड़ में आगे रहने के लिए कोयले की जगह प्राकृतिक गैस पर निर्भरता इस कदर बढ़ा चुकी हैं कि वहां नेचुरल गैस की कीमतें आसमान पर हैं।
यूरोप और अमेरिका के प्राकृतिक गैस पर ही केंद्रित होने के कारण ऊर्जा का यह संसाधन आक्रामक कूटनीतिक सौदेबाजी का भी जरिया बन चुका है। कुछ इसी राह पर पिछले महीने चीन ने भी कदम बढ़ाया है। ड्रैगन ने अचानक दूसरे देशों में कोयला आधारित परियोजनाओं पर आर्थिक सहयोग से कदम पीछे हटा लिया। इससे दुनिया भर में ऊर्जा संसाधनों का असंतुलन पैदा हो रहा है।
हरित वित्त पोषण की दरकार : एक अनुमान के मुताबिक विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को तत्काल 100 अरब डालर का हरित कोष मुहैया कराया जाना चाहिए। अमीर देश विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के नाम पर हरित ऊर्जा के बड़े लक्ष्य पूरे होते देखना चाहते हैं, लेकिन वे विकासशील देशों को महंगी हरित ऊर्जा परियोजनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का कोई साझा तंत्र विकसित करने में नाकाम हैं। यहां तक कि तकनीक हस्तांतरण के मुद्दे पर भी विकसित देशों का दोहरा रवैया रहा है। ऐसे समय में हरित वित्त पोषण को लेकर साझा नीति तैयार करनी होगी।